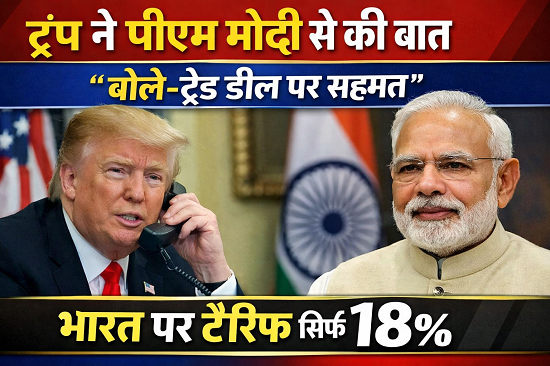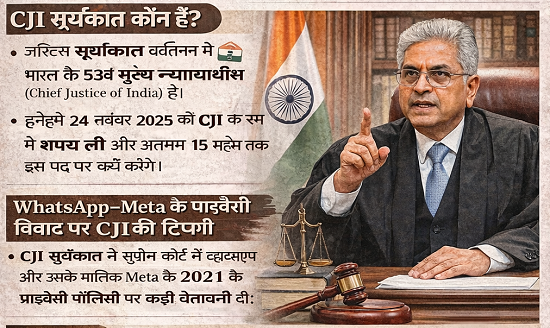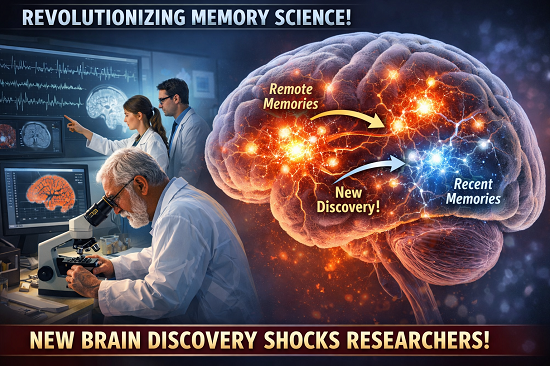नई दिल्ली। लोकसभा की प्रवर समिति ने आयकर विधेयक, 2025 के मसौदे में 32 विशिष्ट मुद्दों की ओर इशारा किया है, जो भारत के कर कानूनों को सरल भाषा में पुनर्लेखन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोमवार को संसद में पेश की गई समिति की रिपोर्ट 4,500 से ज़्यादा पृष्ठों की है और इसमें मसौदा तैयार करने में विसंगतियों, छूटे हुए प्रावधानों और कमियों की ओर इशारा किया गया है, जिनका व्यक्तियों और संगठनों, दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इस साल फरवरी में पेश किया गया यह विधेयक, 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेने और कानून की भाषा और संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। हालांकि, भाजपा सांसद जय पांडा के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, कानूनी पाठ को सरल बनाना स्पष्टता या निष्पक्षता सुनिश्चित करने के समान नहीं है।
रिपोर्ट में सबसे पहले परिभाषाओं पर ध्यान दिया गया है, जिनमें से कई जैसा कि पैनल का कहना है या तो अनावश्यक रूप से अस्पष्ट हैं या उन कानूनों के अनुरूप नहीं हैं जिन्हें वे प्रतिबिंबित करने के लिए हैं। उदाहरण के लिए “पूंजीगत संपत्ति” की परिभाषा में विदेशी संस्थागत निवेशों के अद्यतन प्रावधान शामिल नहीं हैं। “सहकारी बैंक”, “बुनियादी ढांचा पूंजी कंपनी”, और “सूक्ष्म एवं लघु उद्यम” जैसे शब्द ऐसे अन्य उदाहरण हैं, जहां या तो अस्पष्टता आ जाती है या संदर्भ पुराने हो गए हैं।
सुझाव सीधा है: अन्य कानूनों का ढीला-ढाला संदर्भ देने के बजाय परिभाषाओं में सीधे प्रासंगिक वैधानिक भाषा को अपनाया जाना चाहिए। इससे आगे चलकर व्याख्या की परेशानी से बचा जा सकता है।
प्रमुख कटौतियों में सुझाए गए बदलाव
रिपोर्ट कई ऐसे खंडों की ओर इशारा करती है जहाँ आय की गणना या कटौतियां कानून के उद्देश्य से भटक सकती हैं। खंड 22, जो गृह संपत्ति से आय से संबंधित है, इसका एक उदाहरण है। इसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि मानक 30 प्रतिशत कटौती लागू करने से पहले नगरपालिका करों को बाहर रखा जाना चाहिए। पैनल का सुझाव है कि स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए।
उन्होंने आवास ऋणों पर निर्माण-पूर्व ब्याज का मुद्दा भी उठाया। विधेयक के वर्तमान संस्करण के अनुसार, यह कटौती केवल स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति तक ही सीमित प्रतीत होती है। पैनल ने इसे किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए भी खोलने की सिफारिश की है।
नियोक्ता पेंशन अंशदान और धर्मार्थ संस्थाओं को दान जैसे अन्य क्षेत्रों में, समिति ने शब्दों में छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान दिया है जिनके अनपेक्षित प्रभाव हो सकते हैं, या तो योग्यता के दायरे में बदलाव हो सकता है या अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है।
छोटे करदाताओं और धर्मार्थ संस्थाओं के लिए राहत की मांग
समिति विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित है कि यह मसौदा कम आय वाले व्यक्तियों या सार्वजनिक ट्रस्ट पर चलने वाले संगठनों को कैसे प्रभावित कर सकता है। एक उल्लेखनीय उदाहरण: छूट सीमा से कम आय वाले करदाताओं को अभी भी केवल टीडीएस रिफंड का दावा करने के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा। पैनल ने इसे अत्यधिक बताते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा है।
गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए वर्तमान कानून में मौजूद कई सुरक्षा प्रावधान मसौदा विधेयक में शामिल नहीं किए गए हैं। “आय के मान्य उपयोग” की अवधारणा, एक ऐसा प्रावधान जो संस्थाओं को देरी से धन लगाने की अनुमति देता है, को हटा दिया गया है। रिपोर्ट में इसे बहाल करने का सुझाव दिया गया है। वे धार्मिक-सह-धर्मार्थ संस्थाओं को दिए जाने वाले गुमनाम दान पर छूट वापस लाने की आवश्यकता की ओर भी इशारा करते हैं।
कुछ खंडों में “आय” के बजाय “प्राप्ति” शब्द का प्रयोग भी इन संस्थाओं के लिए कराधान की गणना के तरीके को बदल सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो यह बदलाव उनकी कर देनदारी को बढ़ा देगा।
कुछ सिफ़ारिशें तकनीकी या प्रशासनिक परिवर्तनों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उनका महत्व है। पैनल ने अनुरोध किया है कि धारा 395, जो टीडीएस प्रमाणपत्रों से संबंधित है, स्पष्ट रूप से “शून्य” कटौती प्रमाणपत्रों की अनुमति दे, एक ऐसा विवरण जो 1961 के कानून में मौजूद था लेकिन यहाँ अनुपस्थित है।
बहीखातों का रखरखाव न करने के मामलों में दंड को अनिवार्य करने को लेकर भी चिंता है। समिति ऐसे दंडों को स्वचालित बनाने के बजाय, कर अधिकारियों को कुछ विवेकाधिकार बहाल करना चाहती है। यह सिफ़ारिश इस विश्वास पर आधारित है कि हर चूक जानबूझकर नहीं होती।
एक और व्यावहारिक सुझाव: अनिवासी संपर्क कार्यालयों को अपने विवरण दाखिल करने के लिए खासकर विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अनुपालन के बोझ को देखते हुए 8 महीने तक का अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव जिसके लिए उन्होंने ज़ोर दिया है, वह है कर-परिहार-विरोधी प्रावधानों के तहत “मामले की परिस्थितियों में” वाक्यांश को बहाल करना। यह मामूली लग सकता है, लेकिन कर विवादों में ऐसी भाषा मायने रखती है।
आगे क्या?
सरकार ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है कि वह समिति के कितने सुझावों को स्वीकार करेगी। लेकिन यह देखते हुए कि यह दशकों में भारत के सबसे बड़े कर कानूनों में से एक है, विधायी प्रारूपण की गुणवत्ता पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, न केवल यह कि कानून कितना पठनीय है, बल्कि यह भी कि यह कितना निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार है।